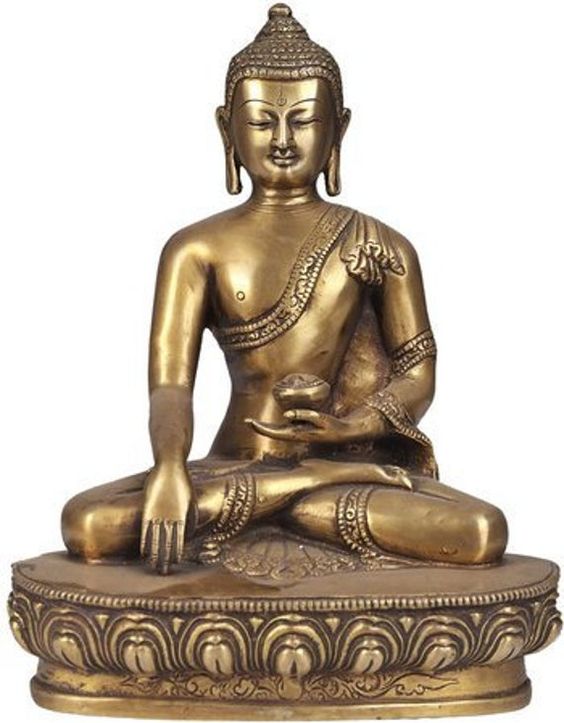बौद्ध धर्म (baudh dharm)
बौद्ध धर्म ( baudh dharm) भारत की श्रमण परम्परा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। इसकी उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसे मानवीय धर्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को महत्व दिया गया है। ईसा पूर्व 6 वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध (baudh dharm ke sansthapak) द्वारा बौद्ध धर्म (baudh dharm) की स्थापना की गयी।
बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुंबिनी जो वर्तमान नेपाल है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर,भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले पाँच शताब्दियों में, बौद्ध धर्म (baudh dharm) पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले दो हजार वर्षों में मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी फैल गया। इन्हें एशिया का ज्योति पुँज भी कहा जाता है।
baudh dharm ka itihas
महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी सम्पूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ उनके सिद्धांत हैं। उनके सभी सिद्धांतों में प्रतीत्य समुत्पाद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है- प्रतीत्य (किसी वस्तु के होने पर) समुत्पाद (किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति)। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं ,जिसे द्वादश निदान कहा जाता है।
प्रतीत्य समुत्पाद एवं द्वादश निदान (12 उपचार)-
यह बौद्ध दर्शन का केन्द्रीय सिद्धांत है। यह बौद्ध दर्शन का कारणता / कार्य – कारण सिद्धांत है। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना एवं कार्य- कारण पर निर्भर रहते हैं।
12 निदान इस प्रकार हैं-
- अविद्या – (अज्ञान – कर्म – दुःख का मूल कारण)
- संस्कार
- विज्ञान – चेतना (भ्रूण) / जन्म
- नामरूप – आत्मा बनती है।
- षङायतन (सलायतन) – 6 इन्द्रिया
- स्पर्श
- वेदना
- तृष्णा
- उपादाान (तीव्र इच्छा)
- भव – जन्म गृहण करने की प्रवृति
- जाति – पुनर्जन्म की इच्छा
- जरा – मरण
गौतम बुद्ध के उपदेश
गौतम बुद्ध के उपदेश Gautam Buddha अनुभव के आग में तप कर सामने आए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध के उपदेश Gautam Buddha Updesh किसी खज़ाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार Gautam Buddha Thoughts आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश, Gautam Buddha Quotes Hindi, बुद्ध के विचार , Gautam Buddha Suvichar को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं।
साथ ही हम बुद्धा कोट्स, Mahatma Budh ki Shiksha, बुद्ध के उपदेश, Bhagwan Buddha ke Vichar के द्वारा हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी गौतम बुद्ध के उपदेश Gautam Buddha Quotes को पढ़ें और इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। गौतम बुद्ध के उपदेश Gautam Buddha Quotes in Hindi एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है।
क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुःख-तकलीफों से मुक्त हो चुका है।
जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकडे रहने के सामान है, इसमें आप ही जलते हैं।
ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थाई नहीं हो सकती। अगर आप अँधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रौशनी की तलाश क्यों नहीं करते।

मध्यमप्रतीपदा (मध्यममार्ग)
मध्मप्रतीपदा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है,जो दो अतिवादी विचारों के बीच का मार्ग है। बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म नहीं है। उदारहण –जीवन में अत्यधिक दुः ख भी नहीं तो अत्यधिक सुख भी नहीं होना चाहिए। शून्यवाद-(माध्यमिक शून्यवाद) महायान बौद्ध धर्म से संबंधित सिंद्धांत । यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था।
प्रत्येक घटना एवं कार्य – कारण पर निर्भर होने के कारण शून्य हैं। अर्थात् उनका संबंध स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
योगाचार विज्ञानवाद-
मौत्रेयनाथ ने इसकी स्थापना की थी। असंग इसके विस्तारक थे। यह सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था।
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त(baudh dharm ke siddhant)
महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक ज्ञान, राजनीतिक, स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी है। बौद्ध धर्म (baudh dharm) मूलतः अनीश्वरवादी अनात्मवादी है अर्थात इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसमें पुनर्जन्म को मान्यता दी गयी है।
4 arya satya in hindi
भगवान बुद्ध द्वारा उद्घघाटित ‘सत्य’ को ‘आर्य सत्य’ के नाम से जाना जाता है। यहाँ आर्य का अर्थ ‘श्रेष्ठ’ है। बुद्ध ने सांसारिक दुःखों के सम्बन्ध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार हैं, अर्थात् बुद्ध के चार सिद्धांत जीवन के ‘श्रेष्ठ सत्य’ हैं। इसका यह अर्थ भी माना जाता है कि ये ‘सत्य’ आर्य(श्रेष्ठ) पुरुष द्वारा उपदिष्ट हैं। बौद्ध-काल में ‘आर्य’ शब्द किसी जाति का सम्बोधन नहीं करते हुए शालीनता और सभ्यता के प्रतीक धे और इसीलिए भगवान बुद्ध के प्रमुख सूत्रों को ‘चार आर्य सत्य’ के नाम से प्रसिद्धि मिली।
जो इस प्रकार हैं-
1. दुःख – संसार में सर्वत्र दुःख है। जीवन दुःखों व कष्टों से भरा है। संसार को दुःखमय देखकर ही बुद्ध ने कहा था- “सब्बम् दुःखम्”।
2. दुःख समुदाय – दुःख समुदाय अर्थात दुःख उत्पन्न होने के कारण हैं। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः दुःख का भी कारण है। सभी कारणों का मूल अविद्या तथा तृष्णा है। दुःखों के कारणों को “प्रतीत्य समुत्पाद” कहा गया है। इसे “हेतु परम्परा” भी कहा जाता है।
प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। अन्य सिद्धान्त इसी में समाहित हैं। बौद्ध दर्शन का क्षण-भंगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न सिद्धान्त है।
प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुयें कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुःख का सामूहिक नाम “जरामरण” है। जरामरण के चक्र (जीवन चक्र) में बारह क्रम हैं- जरामरण, जाति (शरीर धारण करना), भव (शरीर धारण करने की इच्छा), उपादान (सांसारिक विषयों में लिपटे रहने की इच्छा), तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन (पाँच इंद्रियां तथा मन), नामरूप, विज्ञान (चैतन्य), संस्कार व अविद्या। प्रतीत्य समुत्पाद में इन कारणों के निदान की अभिव्यंजना की गई है।
3. दुःख निरोध – दुःख का अन्त सम्भव है। अविद्या तथा तृष्णा का नाश करके दुःख का अन्त किया जा सकता है।
4. दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा – अष्टांगिक मार्ग ही दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा हैं।
बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग(baudh dharm ke ashtangika marga)
सांसारिक दुःखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात कही है। बौद्ध धर्म के अनुसार, चौथे आर्य स्त्य का आर्य अष्टाण्ग मार्ग है दुःख निरोध पाने का रास्ता । गौतम बुद्ध कहते थे कि चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट होने लगती है और वह निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाता है।
अष्टांगिक मार्ग के साधन हैं-
- सम्यक दृष्टि – वस्तुओं के वास्तविक रूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है।
- सम्यक संकल्प – आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना।
- सम्यक वाक – अप्रिय वचनों का परित्याग।
- सम्यक कर्मान्त – दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना।
- सम्यक आजीव – सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना।
- सम्यक व्यायाम – विवेकपूर्ण प्रयत्न करना।
- सम्यक स्मृति – सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना।
- सम्यक समाधि – चित्त की एकाग्रता
अष्टांगिक मार्ग के साधनों को तीन स्कन्धों में बांटा गया है-
प्रज्ञा – सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक
शील – सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम
समाधि – सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि
बुद्ध ने मध्यम मार्ग अथवा मध्यम प्रतिपदा का उपदेश देते हुए कहा कि- “मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं कायाक्लेश से बचना चाहिए” अर्थात न तो अत्यधिक इच्छाएं करनी चाहिए और न ही अत्यधिक तप (दमन) करना चाहिए। बल्कि इनके बीच का मार्ग अपना कर दुःख निरोध का प्रयास करना चाहिए।
शिक्षापाद-: बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अधिक बल दिया गया। दस शीलों का पालन सदाचारी तथा नैतिक जीवन का आधार है। इन शीलों को शिक्षापाद भी कहा जाता है।
- अहिंसा
- सत्य
- अस्तेय (चोरी न करना)
- समय से भोजन ग्रहण करना
- मद्य का सेवन न करना
- ब्रह्मचर्य का पालन करना
- अपरिग्रह (धन संचय न करना)
- आराम दायक शैय्या का त्याग करना
- व्यभिचार न करना
- आभूषणों का त्याग करना
गृहस्थ बौद्ध अनुयायियों को केवल प्रथम पाँच शीलों का अनुशीलन आवश्यक था। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया, उसे ‘उपासक धर्म’ कहा गया।
बौद्ध दर्शन तीन मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है-
- अनीश्वरवाद
- अनात्मवाद
- क्षणिकवाद
यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है।
1. अनीश्वरवाद
बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम पर चलती है। प्रतीत्यसमुत्पाद अर्थात कारण-कार्य की श्रृंखला। इस श्रृंखला के कई चक्र हैं जिन्हें बारह अंगों में बाँटा गया है। अत: इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है। न ही कोई उत्पत्तिकर्ता, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है। तब न कोई प्रारंभ है और न अंत।
2. अनात्मवाद
अनात्मवाद का यह मतलब नहीं कि सच में ही ‘आत्मा’ नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं, वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखरकर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है।
स्वयं के होने को जाने बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। निर्वाण की अवस्था में ही स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महा सुसुप्ति में खो जाती है। वह अनंतकाल तक अंधकार में पड़ी रह सकती है या तक्षण ही दूसरा जन्म लेकर संसार के चक्र में फिर से शामिल हो सकती है। अत: आत्मा तब तक आत्मा नहीं जब तक कि बुद्धत्व घटित न हो। अत: जो जानकार हैं वे ही स्वयं के होने को पुख्ता करने के प्रति चिंतित हैं।
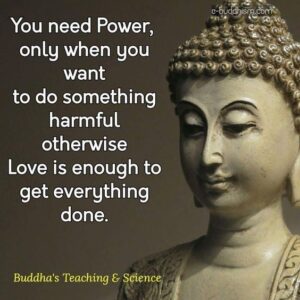
3. क्षणिकवाद
इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। कुछ भी स्थायी नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं और इन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता।
for upsc, bpsc, rrb, ntpc, or any exam se related
उक्त तीन सिद्धांत पर आधारित ही बौद्ध दर्शन की रचना हुई। इन तीन सिद्धांतों पर आगे चलकर थेरवाद, वैभाषिक, सौत्रान्त्रिक, माध्यमिक (शून्यवाद), योगाचार (विज्ञानवाद) और स्वतंत्र योगाचार का दर्शन गढ़ा गया। इस तरह बौद्ध धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदायों के कुल छह उपसम्प्रदाय बने। इन सबका केंद्रीय दर्शन रहा प्रतीत्यसमुत्पाद।